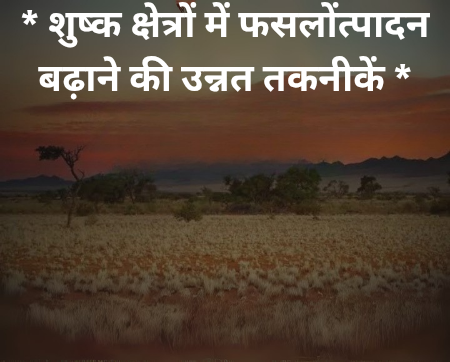
शुष्क क्षेत्रों में फसलोंत्पादन बढ़ाने की उन्नत तकनीके
( क) वर्षा जल का संचयन व संरक्षण
* ढ़लान वाले क्षेत्रों में जल अधिग्रहण क्षेत्र का विकास करना,जिससे मृदा में वर्षा का पानी संचय करने तथा भू-जल स्तर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी ।
* ज्यादा ढ़ालू खेतों में थोड़ी-थोड़ी दूर पर कम ऊंचाई की मेड़ बनाकर पानी के बहाव को कम किया जा सकता है जिससे पानी को जमीन में जाने के लिए अधिक समय मिलेगा ।
* खेत से जो पानी बहकर जावे उसे रोककर कुएं में डालने से कुएँ के जल स्तर में बढ़ोत्तरी की जा सकती है।
* ढ़लान वाले खेतों में कृषि का पाट्टीदार तरीका काम में लेना चाहिए। इसके अंतर्गत बाजार, ज्वार, मक्का आदि अनाज वाली फसलों की कतारों के बाद मूंग, उड़द,मूंगफली, सोयाबीन आदि फसलों की कतारों में बुवाई करते हैं। इन दलहनी व तिलहन फसलों की खासियत यह है कि ये पानी के बहाव को कम करती है जिसे उपजाऊ मिट्टी का कटाव तो रुकता ही है जमीन में पानी का रिसाव भी बढ़ता है।
* खेत के निचले इलाकों में तालाब व टैंक का निर्माण करके वर्षा के पानी को इकट्ठा करना और उसका फसल की संवेदनशील अवस्थाओं पर सिंचाई के लिए प्रयोग करना ।
- शुष्क क्षेत्रों में फसलोंत्पादन बढ़ाने की उन्नत तकनीके व जैसे भू- समतलीकरण , वृक्षारोपण, मेड़बंदी व ढलान के विपरीत जुताई व बुवाई करके वर्षा के पानी को बहकर नहीं जाने देना चाहिए और साथ ही पानी से होने वाले मृदा कटाव को रोकना चाहिए खेत की ढ़लान के विपरीत खेती करने अर्थात समस्त कृषि क्रियाएं जैसे जुताई ,बुवाई आदि खेत की ढलान के आड़े की जावे तो कुंड का पानी कुंड में तथा खेत का पानी खेत में ही रहता है तथा व्यर्थ बहकर नहीं जाता। इस तरह ज्यादा से ज्यादा पानी जमीन के अंदर जाता है जो कि वर्षा समाप्त होने के बाद फसल के लिए लंबे समय तक काम आता है।

* संरक्षित कृषि पद्धतियों व पलवार( घास से ढकना) के उपयोग को बढ़ाना।
* भूमि में अधिक जल अवशोषित करने के लिए गहरी जुताई, मेड़ बनाना व ढलान के विपरीत बुवाई आदी तकनीकों को अपनाना।
( ख) मृदा नमी संरक्षण
* खरपतवार,मृदा नमी को वाष्पोत्सर्जन करके उड़ा देते हैं।अतः बरानी क्षेत्रों में सफल कृषि प्रबंधन के लिए, खरपतवारों से वाष्पोत्सर्जन को रोकने व फसलों को उचित जगह,प्रकाश एवं पोषण प्रदान करने के लिए समुचित खरपतवार नियंत्रण आवश्यक है।
* गर्मी में गहरी जुताई करें व वर्षा उपरान्त जुताई करके पटा लगाकर मृदा नमी संरक्षण करना चाहिए । भारी और दोमट मृदा वाले क्षेत्रों में गर्मी की जुताई करने से भूमि में अधिक जल सोखने की क्षमता बढ़ती है। जमीन से पानी को भाप बनकर उड़ाने से रोकने के लिए कुल्फा व बक्खर चलाकर मिट्टी की उपरी परत को तोड़ देना चाहिए। यह टूटी हुई परत सतह आवरण का काम करती है ।
* वाष्पीकरण द्वारा होने वाली नमी ह्नास को कम करने के लिए पलवार (मल्च) का प्रयोग करें।
* पत्तियो को मुरझाने से बचाने के लिए पोटेशियम का पर्णीय छिड़काव (0.5 प्रतिशत) तथा पुरानी पत्तियों को निकाल दे ।
* उचित पौधों की संख्या बनाए रखें यदि पौधे घने हो तो और मृदा में नमी को देखते हुए कुछ पौधे उखाड़ दें।
* मृदा जल धारण क्षमता, मृदा उर्वरता व कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के लिए 5 -10 टन प्रति हेक्टर गोबर की खाद कम्पोस्ट 5 से 8 टन प्रति हेक्टर,वर्मी कम्पोस्ट 3 से 6 टन प्रति हेक्टेयर एवं फसल अवशेषों का प्रयोग करें।
* मध्यकालीन सुधार करें जिसे अन्तः सस्य क्रियाएँ, से क्रिया पौधों की संख्या कम करना, जीवन रक्षक सिंचाई आदि करना ।
* मृदा नमी संरक्षण के लिए पॉलीमर्स का प्रयोग करें जैसे-हाइड्रोजेल (2.5 से 5.0 किलोग्राम प्रति हैक्टर) I
* वाष्पोत्सर्जनरोधी रसायनों जैसे केओलिन 6% साइको से 0.03% का फसल की उचित अवस्था में छिड़काव करें ।

मल्चिंग द्वारा शुष्क क्षेत्र में फसलोत्पादन
(ग) उपलब्ध मृदा नमी का दक्ष प्रयोग
* सुखारोधी फसलों व किस्मों का चयन कर बारानी क्षेत्रों की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है ।
* शुष्क व अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में उपयुक्त फसल प्रणालियों से प्राप्त होने वाली उपज और शुद्ध लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है।
* उपयुक्त बुवाई विधियों जैसे सही समय पर फसल की बुवाई व सही गहराई पर बीज का डालना, पानी के साथ बुवाई को अपनाना, या पौरा/ केरा द्वारा कुड़ो में में बुवाई। रबी में देश के उत्तर-पश्चिम भागों में जहाँ बुवाई के समय नमी कम पाई जाती है वहाँ बुवाई के समय एक्वा हल से 15,000 से 20,000 लीटर प्रति हेक्टर की दर से पानी के साथ बुवाई करने से अंकुरण व फसल स्थापन ठीक आ जाता है तथा फसल का अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है।
* उर्वरकों का सही समय, सही मात्रा व उपयुक्त गहराई पर प्रयोग करें।
* खड़ी फसल में यूरिया का छिड़काव 1 से 2% या भायो- यूरिया 0.1% का छिड़काव करें।
* बीज के अच्छे अंकुरण के लिए पानी या पोटेशियम नाइट्रेट के द्वारा बीजोपचार करके बुवाई करें।
* फसल की अवधि के दौरान नमी उपलब्ध होने पर उर्वरकों का उपयोग करें।

( घ ) समेकित पोषक तत्व प्रबंधन
* असिंचित क्षेत्रों की मृदाऐ प्यासी ही नहीं परन्तु भूखी भी रहती है। क्योंकि इन क्षेत्रों में मृदा व जल अपरदन के कारण तथा कम पोषक तत्वों के प्रयोग से मृदा उर्वरकता कमजोर रहती है। कृषि उत्पादकता, मृदा उर्वरकता तथा पर्यावरण संरक्षण को एक साथ समावेशित करने के लिए समेकित या एकीकृत पादप पोषक तत्व प्रबंधन की आवश्यकता है। समेकित पादप पोषक तत्व प्रबंधन से अभिप्राय यह है कि फसल उत्पादकता एवं मृदा उर्वरकता को बढ़ाने तथा बनाए रखने के लिए पोषक तत्वों के सभी उपलब्ध स्रोतों (उर्वरक जीवांश/ कार्बनिक खादें, पौधों एवं जीवों के अवशेष, औद्योगिक उपउत्पाद,जैविक उर्वरक आदि ) से मृदा में पोषक तत्वों का इस प्रकार सामजस्य कि जैविक गुणवत्तता से पर हानिकारक प्रभाव डाले बगैर लगातार उच्च आर्थिक उत्पादन लिया जा सकें । यह निर्विवाद सत्य है कि कार्बनिक खादों के साथ-साथ रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग से न केवल अधिकतम उपज ली जा सकती है , बल्कि लम्बे समय तक इनके प्रयोग से भूमि के उर्वरता स्तर में भी सुधार होता है । कार्बनिक खादें जैसे गोबर की खाद( 5-10 टन /हेक्टर), कम्पोस्ट(5-8 टन/हैक्टर), वर्मीकम्पोस्ट (3-6 टन/हैक्टर), हरी खाद जैसे ढ़ैचा, ग्वार इत्यादि ,फसल आवशेष, जैव-उर्वरक आदि का प्रयोग करने से भूमि की उर्वरा-शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है। इसके अतिरिक्त कार्बनिक खादों के प्रयोग से मृदा में निम्नलिखित लाभ है :-
* कार्बनिक खादों में पोषक तत्व घुलनशील अवस्था में रहते हैं एवं इस खाद में मृदा की प्राकृतिक उर्वरा शक्ति को फिर से जीवित करने की सामर्थता मौजूद होती है। इसलिए इस खाद को प्रयोग करने के बाद इसका असर लंबे समय तक बना रहता है।
* अपने दानेदार प्रकृति के कारण कार्बनिक खाद व वर्मी कम्पोस्ट भूमि के वायु परिसंचरण, जलधारण क्षमता को न केवल सुधरता है अपितु जड़ बढ़ाव व फैलाव में वृद्धि भी करता है।
* कार्बनिक खादों व वर्मी कम्पोस्ट के प्रयोग से मृदा की जलधारण क्षमता में वृद्धि होती है व सिंचाई में बचत होती हैं l
* कार्बनिक खादों व वर्मी कम्पोस्ट में बहुत से ह्युमिक एसिड्स रहते हैं जिनका कार्य पौधों की बढ़वार में वृद्धि के साथ ही केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी व भूमि की भौतिक दशा सुधार ना होता है।
* कार्बनिक खादों के प्रयोग से फल, सब्जियों व अनाज की गुणवत्ता में सुधार कर कृषक की उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त किया जा सकता है ।
( ड़ ) शुष्क एवं अर्द्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त जल प्रबंधन प्रौद्योगिकी
* नवीनतम सिंचाई विधियों जैसे स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई विधि से सामान्य विधि एवं खासकर अधिक मूल्य वाली फसलों में अधिक जल उपयोग क्षमता में कम जल का प्रयोग और अधिक पैदावार के साथ-साथ कृषि आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि होती है।
* ड्रिप (बूँद – बूँद) सिंचाई विधि विभिन्न फसलों में उच्च गुणवत्ता एवं अधिक पैदावार के लिए अति उत्तम साबित हुई है। अतः किसान इस सिंचाई विधि की अधिक प्रारंभिक लागत के कारण विभिन्न केंद्रीय राज्य सरकार की योजनाओं से ऋण, अनुदान एवं सुविधाओं का उचित लाभ उठाकर ड्रिप सिंचाई प्रणाली को अपनाकर अधिक धनोपाजर्न वाली फसलों में जल उपयोगि दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ उच्च गुणवत्तायुक्त अधिक उत्पादन एवं लाभ ले सकते हैं।
* स्प्रिंकलर व ड्रिप सिंचाई विधि खेतों में लगाए जाने वाली सामान्यतः सभी फसलों जैसे कि गेहूँ, आलू, सब्जियां,दलहनी व तिलहनी फसलों आदि के लिए कम जल उपलब्धता, असमतल,उबड़-खाबड़ एवं पहाड़ी क्षेत्रों के साथ-साथ लवणीय मृदाओं में कृषि उत्पादन व उच्च जल दक्षता के लिए एक अच्छा विकल्प है।
* स्प्रिंकलर और ड्रीप उद्यान , कृषि-उद्यानिकी एवं कृषि-वानिकी कृषि प्रणालियों में उच्च जल क्षमता, गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादन एवं अधिक लाभ के लिए अच्छी जल प्रबंधन तकनीकें है |
* जल प्रबंधन के लिए उपयुक्त फसल क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई देनी चाहिए। अगर गेहूं के लिए एक ही सिंचाई जल की उपलब्धता हो तो क्राउन जड़ की शुरुआती ( सी .आर.आई.) अवस्था पर सिंचाई अवश्य करें । अगर दो सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता हो तो (सी .आर.आई.) व फुल व्यवस्था पर सिंचाई करें ।( च ) समेकित खरपतवार प्रबंधन
* खरपतवार ने केवल फसल से वृद्धि व स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं बल्कि फसलों के हिस्से के जल व पोषक तत्वों का भी अवशोषण करते हैं । खरपतवार, मृदा नमी को वाष्पोत्सर्जन करके उड़ा देते हैं। अतः असंचित क्षेत्रों में सफल कृषि प्रबंधन के लिए खरपतवारों का नियंत्रण अति आवश्यक है। खरपतवारों का प्रकोप कम हो इसके लिए बुवाई से पूर्व जुताई व खेत की तैयारी भली प्रकार से करें। यदि शुन्य जुताई विधि द्वारा बुवाई की हो तो फसल में पूर्व फसलों के अवशेषों का आवरण बनाकर रखें ।
फसल अवशेषों का आवरण ( पलवार ) खेत में बनाए रखने से खरपतवारों का अंकुरण कम होता है तथा मृदा नमी का ह्नास भी कम होता है जब फसल 20 से 40 दिन की हो जाए तब आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करने से खरपतवार नियंत्रण के अतिरिक्त भूमि की ऊपरी परत टूट जाने से मृदा नमी का वाष्पीकरण कम होता है तथा मृदा में वायु संचार भी बढ़ता है। विभिन्न फसलों के लिए आवश्यकता अनुसार उपयुक्त समय परशाकनाशियों का प्रयोग करके भी खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है।
